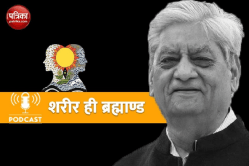Friday, July 25, 2025
संस्कृति और परंपराओं से जुड़े नाट्यकर्म के संवाहक रहे
डॉ. राजेश कुमार व्यास
संस्कृतिकर्मी, कवि और कला समीक्षक
जयपुर•Jul 24, 2025 / 06:00 pm•
Neeru Yadav
रतन थियम मणिपुर के थे पर अपने नाटकों में उन्होंने भारतीय कला-दृष्टि को निंरतर पुनर्नवा किया। संस्कृति और परम्पराओं से जुड़ा उनका नाट्यकर्म इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि उसमें समय-संदर्भों को सहेजते हुए आधुनिक दृष्टि समाई हुई थी। पारम्परिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य, धार्मिक अनुष्ठान, युद्ध कला, रंजन से जुड़े हमारे प्राचीन तत्त्वों और संस्कृत नाटकों के सौंदर्य सिद्धान्तों के आलोक में युगीन परिवेश को घोलकर नाट्य को जिन निर्देशकों ने भारतीयता से जोड़ा उनमें रतन थियम महत्त्वपूर्ण कड़ी थे।
पश्चिमी रंगकर्म के घटाटोप में रंगकर्म को हमारी प्रदर्शनकारी कलाओं की जड़ों से सींचते रतन थियम ने नाट्य प्रदर्शन के बुनियादी आधार-निर्देशक, रंग शिल्प और अभिनय, इनकी त्रिवेणी में भारतीय रंगमच को अपनी मौलिक दृष्टि से विकसित किया। नाट्य पाठ को संवाद से ही जीवंत करने की रूढ़ परम्परा को तोड़ते उन्होंने उसमें निहित भाव और छिपे हुए युगीन संदर्भों के आलोक में नाट्य प्रदर्शन के सौंदर्य का नया मुहावरा रचा। उनके निर्देशित ‘करणभारम्’, ‘इम्फाल इम्फाल’, ‘चक्रव्यूह’, ‘उत्तर प्रियदर्शी’, ‘ऋतुसंहारम्’ आदि बहुत से नाटकों की प्रदर्शन-दीठ में जाएंगे तो यह भी पाएंगे कि उन्होंने समकालीन संदर्भों में भारतीय मूल्यों और मान्यताओं को आधुनिक संदर्भ देते रंगकर्म की अपनी सामाजिकी गढ़ी। यह ऐसी है जिसमें पौराणिक, धार्मिक आख्यानों में निहित कथाओं की आधुनिक कहन-दृष्टि समाई है।
रतन थियम रंगकर्म में संप्रेषण की गहन गत्यात्मकता से जुड़े थे। बहुत से उनके नाटक देखने इसलिए भी जाना हुआ कि वहां पर बंधी-बंधाई कथाओं की रूढ़ परम्पराओं से इतर नाट्य की वह वैचारिकी मिलती थी जिसमें संगीत, अभिनय छटाएं, कहने की लय, नृत्यमूलक दैहिक गतियां, देखने का अनूठा उजास हमें सौंपती थी। सुनी-सुनाई, पढ़ी-पढ़ाई कथाओं में भी कैसे आधुनिक समय को गूंथा जाता है, यह रतन थियम अपने नाटकों से जैसे समझाते थे। शायद इसलिए कि जितना उनका लेखन से नाता था, उतना ही संगीत, नृत्य और दूसरी कलाओं से भी था। यह था, तभी तो कलाओं के अन्त:संबंधों की विरल दृष्टि में रंगकर्म का सर्वथा नया शिल्प वह गढ़ पाए। यह ऐसा था जिसमें नाट्य देखते हम काव्य की लय, चित्रकला सी दृश्यात्मकता और नृत्य की गतियों में देह—विसर्जन को गहरे से अनुभूत करते थे।
असल में रतन थियम ने नाट्य प्रदर्शन में सदा नए रूपों का अन्वेषण किया। गहरी सांस्कृतिक चेतना के साथ कला के सौंदर्यबोध को अपने नाटकों में जिया। इसलिए उनके नाटक युगीन सार्थकता और प्रामाणिकता के साथ ऐसा रूप-बंध है, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी रंगकर्म में घुलकर नाटक जीवन से जुड़ सार्वभौमिक हो उठता है। वह कहते भी थे, ‘मणिपुर से आता हूं, पर अपने नाटकों के जरिए मैं विश्व से संवाद करता हूं।’
यह महज संयोग ही नहीं है कि मणिपुर के दो विरोधाभाषी समुदायों की सर्वथा भिन्न परम्पराओं, मान्यताओं और दृष्टियों के बावजूद उन्होंने उनमें निहित मानवीय मूल्यों को एक-दूसरे में साझा करते अपने नाटकों में प्रत्यक्ष-अपरोक्ष उसे जिया है। नौ पहाड़ों से घिरी हुई एक घाटी के आलोक में ‘नाईन हिल्स वन वैली’ नाटक का संदर्भ देते हुए वह वहां रहने वाले लोगों ‘नागू’ का हवाला देते हैं कि यह लोग बाहरी दुनिया को भी देखते हैं और उनके साथ जो घटित हो रहा है, उसे भी। वहां की चालीस से अधिक जनजातियों, उनकी बोलियों, अनुष्ठान, कलाओं को सहेजते वह समय के साथ प्रकृति सरीखे उल्लास में जीने वाले लोगों की औचक बढ़ती उदासी, डर, गायब होती मुस्कान आदि को दूसरे प्रांतों में भी जीवित पाते और भविष्य के लिए उठने वाले प्रश्नों में जिया है। रंगकर्म को उन्होंने इधर सामयिक मुद्दों से निंरतर जोड़ा। इस दृष्टि से उनका संपूर्ण रंगकर्म परम्परा में गूंथी सामाजिकी ही है। नाट्य की आंतरिक ताकत को पहचानते उसे सामाजिक जागरण से उन्होंने जोड़ा।
प्रदर्शन की परम्परागत सौंदर्य दृष्टि में सर्वथा नई वह वैचारिकी हमें सौंपी, जिसमें नाटक प्रदर्शन के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कला-रूप बनता हममें बसता है। मणिपुर की संकीर्तन और दूसरी धार्मिक परम्पराओं, अनुष्ठानों के आलोक में उन्होंने नाट्यशास्त्र में निहित लोक के आलोक की विश्व-दृष्टि हमें दी है। इम्फाल में उन्होंने ‘कोरस रेपेट्री थियेटर’ रंगमंडल की स्थापना कर जब ‘चक्रव्यूह’ जैसा बहुचर्चित नाटक प्रदर्शित किया तो घूम—घूमकर उसके लिए अभिनेताओं की तलाश की। मणिपुर के साथ चीन, बरमा, थाइलैण्ड की रंगपरम्पराओं के साथ लोक से जुड़ी भारतीय परम्परा के साथ उन्होंने अपने नाटकों में भारत-भर के राज्यों में लोक नाट्यों, रंग—परम्पराओं की सौंधी महक को अपने प्रदर्शन में घोला। संस्कृत नाटकों में निहित गूढ़ अर्थों में जाते उन्होंने पौराणिक पात्रों को ? नवीन अर्थ, सामयिक संदर्भ दिए। वह राष्ट्रीय नाट्यविद्यालय के विद्यार्थी रहे और बाद में वहीं के निदेशक और बाद में अध्यक्ष भी रहे। उनका बिछोह रंगकर्म की भारतीय दृष्टि, शास्त्रीय और लोक में गूंथे नाट्यशिल्प की आधुनिकी के एक युग का अवसान है।
पश्चिमी रंगकर्म के घटाटोप में रंगकर्म को हमारी प्रदर्शनकारी कलाओं की जड़ों से सींचते रतन थियम ने नाट्य प्रदर्शन के बुनियादी आधार-निर्देशक, रंग शिल्प और अभिनय, इनकी त्रिवेणी में भारतीय रंगमच को अपनी मौलिक दृष्टि से विकसित किया। नाट्य पाठ को संवाद से ही जीवंत करने की रूढ़ परम्परा को तोड़ते उन्होंने उसमें निहित भाव और छिपे हुए युगीन संदर्भों के आलोक में नाट्य प्रदर्शन के सौंदर्य का नया मुहावरा रचा। उनके निर्देशित ‘करणभारम्’, ‘इम्फाल इम्फाल’, ‘चक्रव्यूह’, ‘उत्तर प्रियदर्शी’, ‘ऋतुसंहारम्’ आदि बहुत से नाटकों की प्रदर्शन-दीठ में जाएंगे तो यह भी पाएंगे कि उन्होंने समकालीन संदर्भों में भारतीय मूल्यों और मान्यताओं को आधुनिक संदर्भ देते रंगकर्म की अपनी सामाजिकी गढ़ी। यह ऐसी है जिसमें पौराणिक, धार्मिक आख्यानों में निहित कथाओं की आधुनिक कहन-दृष्टि समाई है।
रतन थियम रंगकर्म में संप्रेषण की गहन गत्यात्मकता से जुड़े थे। बहुत से उनके नाटक देखने इसलिए भी जाना हुआ कि वहां पर बंधी-बंधाई कथाओं की रूढ़ परम्पराओं से इतर नाट्य की वह वैचारिकी मिलती थी जिसमें संगीत, अभिनय छटाएं, कहने की लय, नृत्यमूलक दैहिक गतियां, देखने का अनूठा उजास हमें सौंपती थी। सुनी-सुनाई, पढ़ी-पढ़ाई कथाओं में भी कैसे आधुनिक समय को गूंथा जाता है, यह रतन थियम अपने नाटकों से जैसे समझाते थे। शायद इसलिए कि जितना उनका लेखन से नाता था, उतना ही संगीत, नृत्य और दूसरी कलाओं से भी था। यह था, तभी तो कलाओं के अन्त:संबंधों की विरल दृष्टि में रंगकर्म का सर्वथा नया शिल्प वह गढ़ पाए। यह ऐसा था जिसमें नाट्य देखते हम काव्य की लय, चित्रकला सी दृश्यात्मकता और नृत्य की गतियों में देह—विसर्जन को गहरे से अनुभूत करते थे।
असल में रतन थियम ने नाट्य प्रदर्शन में सदा नए रूपों का अन्वेषण किया। गहरी सांस्कृतिक चेतना के साथ कला के सौंदर्यबोध को अपने नाटकों में जिया। इसलिए उनके नाटक युगीन सार्थकता और प्रामाणिकता के साथ ऐसा रूप-बंध है, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी रंगकर्म में घुलकर नाटक जीवन से जुड़ सार्वभौमिक हो उठता है। वह कहते भी थे, ‘मणिपुर से आता हूं, पर अपने नाटकों के जरिए मैं विश्व से संवाद करता हूं।’
यह महज संयोग ही नहीं है कि मणिपुर के दो विरोधाभाषी समुदायों की सर्वथा भिन्न परम्पराओं, मान्यताओं और दृष्टियों के बावजूद उन्होंने उनमें निहित मानवीय मूल्यों को एक-दूसरे में साझा करते अपने नाटकों में प्रत्यक्ष-अपरोक्ष उसे जिया है। नौ पहाड़ों से घिरी हुई एक घाटी के आलोक में ‘नाईन हिल्स वन वैली’ नाटक का संदर्भ देते हुए वह वहां रहने वाले लोगों ‘नागू’ का हवाला देते हैं कि यह लोग बाहरी दुनिया को भी देखते हैं और उनके साथ जो घटित हो रहा है, उसे भी। वहां की चालीस से अधिक जनजातियों, उनकी बोलियों, अनुष्ठान, कलाओं को सहेजते वह समय के साथ प्रकृति सरीखे उल्लास में जीने वाले लोगों की औचक बढ़ती उदासी, डर, गायब होती मुस्कान आदि को दूसरे प्रांतों में भी जीवित पाते और भविष्य के लिए उठने वाले प्रश्नों में जिया है। रंगकर्म को उन्होंने इधर सामयिक मुद्दों से निंरतर जोड़ा। इस दृष्टि से उनका संपूर्ण रंगकर्म परम्परा में गूंथी सामाजिकी ही है। नाट्य की आंतरिक ताकत को पहचानते उसे सामाजिक जागरण से उन्होंने जोड़ा।
प्रदर्शन की परम्परागत सौंदर्य दृष्टि में सर्वथा नई वह वैचारिकी हमें सौंपी, जिसमें नाटक प्रदर्शन के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कला-रूप बनता हममें बसता है। मणिपुर की संकीर्तन और दूसरी धार्मिक परम्पराओं, अनुष्ठानों के आलोक में उन्होंने नाट्यशास्त्र में निहित लोक के आलोक की विश्व-दृष्टि हमें दी है। इम्फाल में उन्होंने ‘कोरस रेपेट्री थियेटर’ रंगमंडल की स्थापना कर जब ‘चक्रव्यूह’ जैसा बहुचर्चित नाटक प्रदर्शित किया तो घूम—घूमकर उसके लिए अभिनेताओं की तलाश की। मणिपुर के साथ चीन, बरमा, थाइलैण्ड की रंगपरम्पराओं के साथ लोक से जुड़ी भारतीय परम्परा के साथ उन्होंने अपने नाटकों में भारत-भर के राज्यों में लोक नाट्यों, रंग—परम्पराओं की सौंधी महक को अपने प्रदर्शन में घोला। संस्कृत नाटकों में निहित गूढ़ अर्थों में जाते उन्होंने पौराणिक पात्रों को ? नवीन अर्थ, सामयिक संदर्भ दिए। वह राष्ट्रीय नाट्यविद्यालय के विद्यार्थी रहे और बाद में वहीं के निदेशक और बाद में अध्यक्ष भी रहे। उनका बिछोह रंगकर्म की भारतीय दृष्टि, शास्त्रीय और लोक में गूंथे नाट्यशिल्प की आधुनिकी के एक युग का अवसान है।
संबंधित खबरें
Hindi News / Opinion / संस्कृति और परंपराओं से जुड़े नाट्यकर्म के संवाहक रहे
यह खबरें भी पढ़ें
लेटेस्ट ओपिनियन न्यूज़
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.