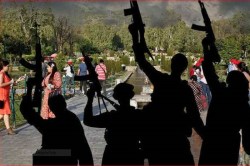Saturday, April 26, 2025
सांस्कृतिक धरोहर : समाज विज्ञानों में शोध के लिए न्याय दर्शन आधारित पद्धति अपनाएं
— डॉ. अमित कुमार दशोरा
(एसोसिएट प्रोफेसर, गलगोटियाज विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा)
जयपुर•Apr 21, 2025 / 12:38 pm•
विकास माथुर
पिछले कुछ वर्षों में योगशास्त्र के महत्त्व को विश्व ने समझा और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रारंभ हुआ। अब यूनेस्को ने श्रीमद्भगवद्गीता तथा नाट्यशास्त्र को ‘मेमोरी ऑफ द वल्र्ड रजिस्टर’ में स्थान दिया है। वैश्विक पटल पर भारतीय शास्त्रों के महत्त्व को अब समझा जाने लगा है। भारतीय शास्त्र सर्वसमावेशी एवं विश्व के कल्याण की सद्भावना से लिखे गए हैं। भारतीय शास्त्रों में सत्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और इस सत्य की खोज के मार्ग भारतीय दर्शन हैं।
संबंधित खबरें
भारतीय चिंतन परंपरा अत्यंत समृद्ध और व्यापक है। हमारे सभी दर्शनों को यदि ध्यान से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि वे मात्र तत्वमीमांसा नहीं हैं, बल्कि विशिष्ट ज्ञान-वर्गों की शोध पद्धतियां हैं। उदाहरण के लिए, न्याय दर्शन सामाजिक विज्ञान की शोध पद्धति के रूप में देखा जा सकता है, योग दर्शन मनोविज्ञान की पद्धति है, मीमांसा व्याख्या की, वैशेषिक भौतिक विज्ञान की, सांख्य प्रकृति और पुरुष के संबंध की तथा वेदांत अखिल ब्रह्मांडीय चेतना की खोज की शोध परंपरा है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में न्याय दर्शन को एक ऐसी शोध पद्धति के रूप में देखा जाता है, जो ज्ञान की उत्पत्ति, उसकी वैधता और सत्य की खोज के लिए तार्किक पद्धतियों को अपनाती है। इसके प्रवर्तक महर्षि अक्षपाद गौतम माने जाते हैं, जिन्होंने लगभग 400 से 600 ईसा पूर्व के मध्य ‘न्याय सूत्र’ की रचना की।
मान्यता है कि गौतम ऋषि सप्त ऋषियों में से एक हैं। अत: वेदों की रचना का कालखंड और गौतम ऋषि का कालखंड एक ही होना चाहिए। गौतम ऋषि का वर्णन रामायण तथा महाभारत दोनों ग्रंथों में भी मिलता है। भारतीय दर्शन को अंग्रेजी में मात्र ‘फिलॉसफी’ कह देने से उनकी पूर्णता और व्यावहारिकता को सीमित कर दिया गया है। जबकि सत्य यह है कि इन दर्शनों में ज्ञान प्राप्ति की विधियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और ये विधियां प्रमाण, तर्क और अनुभव पर आधारित हैं। विशेष रूप से न्याय दर्शन में शोध की जो प्रक्रिया दी गई है, वह आज की शोध पद्धतियों की अनेक सीमाओं को दूर कर सकती है। पिछली लगभग दो शताब्दियों में पश्चिमी शोध पद्धतियों का वर्चस्व रहा है। किंतु अब यह अनुभव किया जा रहा है कि विशेषत: सामाजिक विज्ञानों में यह पद्धतियां अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई हैं। समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, प्रबंधन या अर्थशास्त्र जैसे विषयों में हजारों शोध हो रहे हैं, लेकिन समाज की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, परिवार संस्था के विघटन, नेतृत्व संकट, बढ़ती मानसिक अस्वस्थता और गहराती आर्थिक विषमता को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
पाश्चात्य शोध पद्धतियों में शोध की प्रक्रिया को ‘थीसिस’, ‘हाइपोथीसिस’, ‘डाटा’, ‘एनालिसिस’, और ‘निष्कर्ष’ जैसे चरणों में बांटा गया है। यह प्रक्रिया विज्ञान में जहां उपयोगी हो सकती है, वहीं सामाजिक विज्ञान में यह जीवन की जटिलताओं और मनुष्यों की बहुआयामी प्रकृति को समाहित नहीं कर पाती। साथ ही, इन पद्धतियों में आप्तवाक्य या अनुभवी विशेषज्ञ की वाणी को कोई विशेष स्थान नहीं मिलता, जिससे गहराई और संदर्भ का अभाव हो जाता है। इन्हीं सीमाओं के बीच भारतीय न्याय दर्शन एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभरता है। ऋषि अक्षपाद गौतम द्वारा प्रतिपादित यह दर्शन, शोध की एक ऐसी विधि प्रस्तुत करता है जो विचार से आरंभ होकर सत्य की प्राप्ति तक पहुंचती है। न्याय दर्शन के अनुसार शोध के 16 अवयव होते हैं—प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान। इन अवयवों के माध्यम से किसी विषय को क्रमश: समझा, विश्लेषित और सत्यापित किया जाता है।
इस दर्शन में चार प्रमाण स्वीकृत हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष वह ज्ञान है जो इंद्रियों के माध्यम से सीधे प्राप्त होता है, अनुमान वह ज्ञान है जो कारण-कार्य संबंध के आधार पर प्राप्त होता है, उपमान के माध्यम से हम किसी अनदेखी वस्तु को किसी ज्ञात वस्तु से तुलना करके जान सकते हैं और शब्द का अर्थ है आप्त पुरुष के वचन-अर्थात वह कथन जो निष्पक्ष, अनुभवसंपन्न, और समाजहितकारी विद्वान द्वारा दिया गया हो। यहां केवल प्रकाशित सामग्री को प्रमाण नहीं माना गया, बल्कि उसकी प्रामाणिकता और बोलनेवाले की गुणवत्ता को ही निर्णायक माना गया। न्याय दर्शन में शोध की प्रक्रिया प्रमेय (विषय) से आरंभ होती है और संशय (संदेह) तथा प्रयोजन (प्रश्न की प्रासंगिकता) के स्पष्ट निर्धारण से आगे बढ़ती है। तर्क और निर्णय के बाद यदि मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो न्याय दर्शन में वाद, जल्प और वितंडा जैसे संवाद-प्रकारों के माध्यम से विमर्श को आगे बढ़ाया जाता है। यदि तर्क दोषपूर्ण हैं, तो हेत्वाभास और छल द्वारा उनका विश्लेषण किया जाता है।
जाति के माध्यम से तुलना की दोषपूर्ण पद्धतियों को पहचाना जाता है और निग्रहस्थान वह अवस्था है, जहां तर्क समाप्त होकर निर्णय स्थिर होता है। इस प्रकार, न्याय दर्शन हमें एक ऐसी शोध पद्धति प्रदान करता है जिसमें विषय की समग्रता, संदर्भ की स्पष्टता और समाज के साथ शोध की जीवंतता बनी रहती है। यह शोध को केवल अकादमिक अभ्यास न बनाकर एक जीवंत प्रक्रिया बना देता है, जो सामाजिक जीवन को दिशा देने की क्षमता रखता है। इसलिए समय आ गया है कि भारतीय समाज विज्ञानों में शोध के लिए न्याय दर्शन आधारित पद्धति को अपनाया जाए। यह पद्धति शोध में गहराई, सत्यता और उपयोगिता का समन्वय करते हुए उसे जन-सरोकार से जोडऩे का कार्य कर सकती है। आने वाले समय में सामाजिक विज्ञान की शोध पद्धति के रूप में विश्व न्याय शास्त्र के महत्त्व को भी समझेगा और अन्य शास्त्रों के साथ-साथ न्यायशास्त्र को भी उचित सम्मान मिलेगा।
Hindi News / Opinion / सांस्कृतिक धरोहर : समाज विज्ञानों में शोध के लिए न्याय दर्शन आधारित पद्धति अपनाएं
यह खबरें भी पढ़ें
लेटेस्ट ओपिनियन न्यूज़
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.