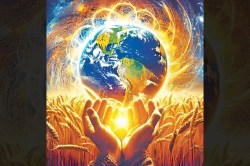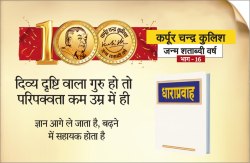Saturday, July 12, 2025
शिक्षा क्रांति भारत के बदलते भविष्य की कुंजी
प्रो. अशोक कुमार, पूर्व कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय
जयपुर•Jul 10, 2025 / 06:25 pm•
Neeru Yadav
शिक्षा क्रांति भारत के बदलते भविष्य की कुंजी है। किसी भी देश के विकास में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्त्वपूर्ण होती है और भारत जैसे युवा और विविधतापूर्ण देश के लिए तो यह और भी आवश्यक है। एक सच्ची शिक्षा क्रांति केवल साक्षरता बढ़ाने से कहीं बढक़र है – यह ज्ञान, कौशल और नवाचार को बढ़ावा देने के बारे में है जो देश को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगी।
वर्तमान शिक्षा की स्थिति को देखते हुए शिक्षा क्रांति की आवश्यकता कई कारणों से है। हरित क्रांति ने जिस तरह कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की, उसी तरह शिक्षा क्रांति का अर्थ शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक और सकारात्मक बदलाव लाना है, ताकि यह सभी के लिए सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और प्रासंगिक बन सके। यह केवल प्रणालीगत सुधारों से नहीं, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण से संभव है, जिसमें प्रौद्योगिकी, नीतिगत बदलाव और सामाजिक सहभागिता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा में जो गहरी असमानताएं मौजूद हैं, खासकर गांव और शहरों के बीच और सरकारी व निजी स्कूलों, महाविद्यालयों , विश्वविद्यालयों के बीच, वे ही शिक्षा क्रांति की सबसे बड़ी आवश्यकता को दर्शाती हैं।
कई ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, खासकर प्राथमिक शिक्षा के बाद। इससे ड्रॉपआउट दर बढ़ती है, खासकर लड़कियों में। कुछ जगहों पर तो प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए स्कूल होते ही नहीं हैं। जहां स्कूल हैं, वहां प्रशिक्षित और पर्याप्त संख्या में शिक्षकों का अभाव एक बड़ी चुनौती है। एक ही शिक्षक को कई कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित होती है। विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी भी एक समस्या है, खासकर विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों में। शिक्षकों का बार-बार तबादला होना भी शिक्षण की निरंतरता को बाधित करता है। सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं का अभाव ! शौचालयों की कमी या गंदगी, पीने के पानी की अनुपलब्धता, जर्जर इमारतें, ब्लैकबोर्ड और बेंच जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव सरकारी स्कूलों की एक बड़ी समस्या है। इन सुविधाओं की कमी से छात्रों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सीखने के माहौल पर नकारात्मक असर पड़ता है। शिक्षण सामग्री और डिजिटल उपकरणों की कमी भी गुणवत्ता को प्रभावित करती है। निजी स्कूल अक्सर बेहतर बुनियादी ढांचा, एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं और आधुनिक शिक्षण विधियों का दावा करते हैं, लेकिन उनकी फीस इतनी अधिक होती है कि समाज के बड़े वर्ग के लिए वे वहनीय नहीं होते। इससे आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के बच्चे तो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। यह शिक्षा तक पहुंच में एक बड़ी असमानता पैदा करता है।
इन सभी कारणों का सीधा परिणाम यह है कि सबको समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। एक बच्चा जो एक सुविधायुक्त निजी स्कूल में पढ़ता है और एक बच्चा जो एक ग्रामीण सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के बिना पढ़ता है, उन्हें कभी समान शैक्षिक अवसर नहीं मिलते। यह न केवल उनके भविष्य के अवसरों को प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी बढ़ाता है।
इसलिए, शिक्षा क्रांति की आवश्यकता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है ताकि इन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। सभी स्कूलों में स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण, पर्याप्त शौचालय, पीने का पानी, बिजली और उचित क्लासरूम सुनिश्चित करना। सभी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना, और उन्हें नई शिक्षण तकनीकों और बाल-केंद्रित शिक्षा के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षित करना। डिजिटल खाई को पाटने के लिए ग्रामीण स्कूलों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल शिक्षण उपकरण उपलब्ध कराना। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को इतना बढ़ाना कि वे निजी स्कूलों के समान या बेहतर विकल्प बन सकें, ताकि आर्थिक स्थिति के बावजूद हर बच्चे को सर्वोत्तम शिक्षा मिले। ऐसी नीतियां बनाना, जो शिक्षा को सभी के लिए सुलभ, सस्ती और समान गुणवत्ता वाली बनाए। जब तक शिक्षा में ये मौलिक असमानताएं दूर नहीं होंगी, तब तक हम एक न्यायपूर्ण और विकसित समाज की कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा क्रांति इन चुनौतियों का समाधान करके प्रत्येक बच्चे के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
दूरदराज के और ग्रामीण इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच अभी भी एक बड़ी समस्या है। परिवहन की कमी, ग्रामीण शिक्षण संस्थानों के लिए अपर्याप्त धन, और इन क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक योग्य शिक्षकों की कमी इस अंतर को बढ़ाती है।
शिक्षा के महत्त्व को जानते हुए भी भारत में बजट में शिक्षा के लिए उचित और पर्याप्त प्रावधान करना एक सतत चुनौती बनी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6त्न खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसके लागू हुए लगभग 5 साल होने को हैं (एनईपी 2020 जुलाई 2020 में जारी हुई थी), और यह लक्ष्य अब भी काफी दूर प्रतीत होता है। जब तक शिक्षा में पर्याप्त निवेश नहीं होगा और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षा क्रांति का सपना अधूरा रहेगा और भ्रम की भावना बनी रहेगी।
एनईपी 2020 के उद्देश्य सराहनीय हैं, जैसे शिक्षा को समावेशी, न्यायसंगत और 21वीं सदी के कौशल के अनुरूप बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का विजन बहुत अच्छा और महत्त्वाकांक्षी है, लेकिन इसके जमीनी हकीकत को समझे बिना और पर्याप्त तैयारी के बिना लागू करने के कारण कई चुनौतियां सामने आई हैं, और यह सच है कि इस वजह से शिक्षा जगत में निराशा और असंतोष का माहौल बना है।
नीति में जो कल्पना की गई है, उसे जमीन पर उतारने में कई बाधाएं आ रही हैं, और यही इसकी विफलता का मुख्य कारण बन रही हैं। नीति को केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर और पर्याप्त संसाधनों के साथ लागू करने की आवश्यकता है। किसी भी बड़ी नीतिगत बदलाव को सफल बनाने के लिए पर्याप्त तैयारी, चरणबद्ध कार्यान्वयन, पर्याप्त वित्तीय आवंटन, शिक्षकों का व्यापक प्रशिक्षण और लगातार मूल्यांकन व सुधार की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी महसूस की जा रही है।
वर्तमान शिक्षा की स्थिति को देखते हुए शिक्षा क्रांति की आवश्यकता कई कारणों से है। हरित क्रांति ने जिस तरह कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की, उसी तरह शिक्षा क्रांति का अर्थ शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक और सकारात्मक बदलाव लाना है, ताकि यह सभी के लिए सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और प्रासंगिक बन सके। यह केवल प्रणालीगत सुधारों से नहीं, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण से संभव है, जिसमें प्रौद्योगिकी, नीतिगत बदलाव और सामाजिक सहभागिता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा में जो गहरी असमानताएं मौजूद हैं, खासकर गांव और शहरों के बीच और सरकारी व निजी स्कूलों, महाविद्यालयों , विश्वविद्यालयों के बीच, वे ही शिक्षा क्रांति की सबसे बड़ी आवश्यकता को दर्शाती हैं।
कई ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, खासकर प्राथमिक शिक्षा के बाद। इससे ड्रॉपआउट दर बढ़ती है, खासकर लड़कियों में। कुछ जगहों पर तो प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए स्कूल होते ही नहीं हैं। जहां स्कूल हैं, वहां प्रशिक्षित और पर्याप्त संख्या में शिक्षकों का अभाव एक बड़ी चुनौती है। एक ही शिक्षक को कई कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित होती है। विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी भी एक समस्या है, खासकर विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों में। शिक्षकों का बार-बार तबादला होना भी शिक्षण की निरंतरता को बाधित करता है। सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं का अभाव ! शौचालयों की कमी या गंदगी, पीने के पानी की अनुपलब्धता, जर्जर इमारतें, ब्लैकबोर्ड और बेंच जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव सरकारी स्कूलों की एक बड़ी समस्या है। इन सुविधाओं की कमी से छात्रों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सीखने के माहौल पर नकारात्मक असर पड़ता है। शिक्षण सामग्री और डिजिटल उपकरणों की कमी भी गुणवत्ता को प्रभावित करती है। निजी स्कूल अक्सर बेहतर बुनियादी ढांचा, एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं और आधुनिक शिक्षण विधियों का दावा करते हैं, लेकिन उनकी फीस इतनी अधिक होती है कि समाज के बड़े वर्ग के लिए वे वहनीय नहीं होते। इससे आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के बच्चे तो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। यह शिक्षा तक पहुंच में एक बड़ी असमानता पैदा करता है।
इन सभी कारणों का सीधा परिणाम यह है कि सबको समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। एक बच्चा जो एक सुविधायुक्त निजी स्कूल में पढ़ता है और एक बच्चा जो एक ग्रामीण सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के बिना पढ़ता है, उन्हें कभी समान शैक्षिक अवसर नहीं मिलते। यह न केवल उनके भविष्य के अवसरों को प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी बढ़ाता है।
इसलिए, शिक्षा क्रांति की आवश्यकता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है ताकि इन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। सभी स्कूलों में स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण, पर्याप्त शौचालय, पीने का पानी, बिजली और उचित क्लासरूम सुनिश्चित करना। सभी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना, और उन्हें नई शिक्षण तकनीकों और बाल-केंद्रित शिक्षा के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षित करना। डिजिटल खाई को पाटने के लिए ग्रामीण स्कूलों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल शिक्षण उपकरण उपलब्ध कराना। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को इतना बढ़ाना कि वे निजी स्कूलों के समान या बेहतर विकल्प बन सकें, ताकि आर्थिक स्थिति के बावजूद हर बच्चे को सर्वोत्तम शिक्षा मिले। ऐसी नीतियां बनाना, जो शिक्षा को सभी के लिए सुलभ, सस्ती और समान गुणवत्ता वाली बनाए। जब तक शिक्षा में ये मौलिक असमानताएं दूर नहीं होंगी, तब तक हम एक न्यायपूर्ण और विकसित समाज की कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा क्रांति इन चुनौतियों का समाधान करके प्रत्येक बच्चे के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
दूरदराज के और ग्रामीण इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच अभी भी एक बड़ी समस्या है। परिवहन की कमी, ग्रामीण शिक्षण संस्थानों के लिए अपर्याप्त धन, और इन क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक योग्य शिक्षकों की कमी इस अंतर को बढ़ाती है।
शिक्षा के महत्त्व को जानते हुए भी भारत में बजट में शिक्षा के लिए उचित और पर्याप्त प्रावधान करना एक सतत चुनौती बनी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6त्न खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसके लागू हुए लगभग 5 साल होने को हैं (एनईपी 2020 जुलाई 2020 में जारी हुई थी), और यह लक्ष्य अब भी काफी दूर प्रतीत होता है। जब तक शिक्षा में पर्याप्त निवेश नहीं होगा और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षा क्रांति का सपना अधूरा रहेगा और भ्रम की भावना बनी रहेगी।
एनईपी 2020 के उद्देश्य सराहनीय हैं, जैसे शिक्षा को समावेशी, न्यायसंगत और 21वीं सदी के कौशल के अनुरूप बनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का विजन बहुत अच्छा और महत्त्वाकांक्षी है, लेकिन इसके जमीनी हकीकत को समझे बिना और पर्याप्त तैयारी के बिना लागू करने के कारण कई चुनौतियां सामने आई हैं, और यह सच है कि इस वजह से शिक्षा जगत में निराशा और असंतोष का माहौल बना है।
नीति में जो कल्पना की गई है, उसे जमीन पर उतारने में कई बाधाएं आ रही हैं, और यही इसकी विफलता का मुख्य कारण बन रही हैं। नीति को केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर और पर्याप्त संसाधनों के साथ लागू करने की आवश्यकता है। किसी भी बड़ी नीतिगत बदलाव को सफल बनाने के लिए पर्याप्त तैयारी, चरणबद्ध कार्यान्वयन, पर्याप्त वित्तीय आवंटन, शिक्षकों का व्यापक प्रशिक्षण और लगातार मूल्यांकन व सुधार की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी महसूस की जा रही है।
संबंधित खबरें
Hindi News / Opinion / शिक्षा क्रांति भारत के बदलते भविष्य की कुंजी
यह खबरें भी पढ़ें
लेटेस्ट ओपिनियन न्यूज़
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.