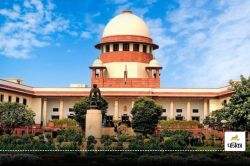Monday, May 19, 2025
छोटे देशों की चिकित्सा शिक्षा गुणवत्ता पर रखनी होगी नजर
भारत में कहीं से भी यानी सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा स्नातक कर रहे विद्यार्थियों का प्रायोगिक ज्ञान स्तर कुछेक विकसित देशों को छोड़कर श्रेष्ठतम होता है। ऐसे में विदेश जा रहे विद्यार्थियों के प्रवाह को लगाम देने के लिए और अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने संबंधी प्रोत्साहन की आवश्यकता है। यदि प्रतिस्पर्धा से डरते हुए एक बाईपास के रूप में इन छोटे देशों में चिकित्सा शिक्षा के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को रोका नहीं गया तो वह भविष्य में चिकित्सा क्षेत्र को प्रभावित करेंगे।
जयपुर•May 19, 2025 / 11:45 pm•
Sanjeev Mathur
डॉ. विवेक एस. अग्रवाल, संचार और शहरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ
दुनिया के छोटे-छोटे देशों में मेडिकल शिक्षा लेकर प्रतिवर्ष हजारों चिकित्सक भारत में प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं। इन देशों में मेडिकल शिक्षा एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रही है। पूर्व सोवियत संघ के विघटन से बने यूक्रेन, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देशों के साथ-साथ चीन, सूडान, यूगांडा, मॉरिशस व नेपाल बड़ी संख्या में और संभवतया अपेक्षित रूप से कम लागत पर चिकित्सा स्नातक तैयार कर रहे हैं। मेडिकल शिक्षा की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व सोवियत संघ के छोटे-छोटे देशों में 10 से 15 तक मेडिकल कॉलेज हैं और उनमें आधे से एक तिहाई तक विद्यार्थी भारतीय ही हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार विगत वर्षों में लगभग 30,000 विद्यार्थी इन छोटे देशों में जाकर चिकित्सा स्नातक के पाठ्यक्रम का हिस्सा बने हैं। एक तरफ जहां भारत में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रैक्टिस करने पर उस राज्य में पंजीकरण कराना होता है, वहीं छोटे देशों में चिकित्सा स्नातक कर ये चिकित्सक कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा देकर प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाते हैं।
दुनिया के छोटे-छोटे देशों में मेडिकल शिक्षा लेकर प्रतिवर्ष हजारों चिकित्सक भारत में प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं। इन देशों में मेडिकल शिक्षा एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रही है। पूर्व सोवियत संघ के विघटन से बने यूक्रेन, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देशों के साथ-साथ चीन, सूडान, यूगांडा, मॉरिशस व नेपाल बड़ी संख्या में और संभवतया अपेक्षित रूप से कम लागत पर चिकित्सा स्नातक तैयार कर रहे हैं। मेडिकल शिक्षा की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व सोवियत संघ के छोटे-छोटे देशों में 10 से 15 तक मेडिकल कॉलेज हैं और उनमें आधे से एक तिहाई तक विद्यार्थी भारतीय ही हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार विगत वर्षों में लगभग 30,000 विद्यार्थी इन छोटे देशों में जाकर चिकित्सा स्नातक के पाठ्यक्रम का हिस्सा बने हैं। एक तरफ जहां भारत में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रैक्टिस करने पर उस राज्य में पंजीकरण कराना होता है, वहीं छोटे देशों में चिकित्सा स्नातक कर ये चिकित्सक कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा देकर प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाते हैं।
संबंधित खबरें
भारत में प्रैक्टिस करने के लिए इन चिकित्सा स्नातकों को साल में दो बार आयोजित होने वाले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (एफएमजीई) में कंप्यूटर पर 300 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के जवाब देने होते हैं और मात्र 50 फीसदी अंकों की प्राप्ति के साथ परीक्षा देने वाला स्नातक किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण के योग्य हो जाता है। इस परीक्षा में किसी भी प्रश्न के गलत होने पर निगेटिव अंक भी नहीं दिए जाते हैं। यानी, कक्षा में पढ़े-लिखे अथवा किताबी ज्ञान के आधार पर विदेशों से स्नातक हुए चिकित्सक सीधे मरीज को इलाज देने के लिए योग्य करार दे दिए जाते हैं। छोटे देशों में पढ़े इन चिकित्सकों की दूरगामी रणनीति में कठिन परिश्रम एवं मरीजों के साथ प्रायोगिक अनुभव रखने वाले भारतीय चिकित्सा स्नातकों के स्नातकोत्तर भर्ती को प्रभावित करना भी होता है। इन चिकित्सकों की रणनीति यह होती है कि वे परीक्षा उत्तीर्ण कर किसी भी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप पूर्ण करते हैं और तत्पश्चात तीन वर्ष सरकारी नौकरी में व्यतीत कर बोनस अंकों के साथ नीट प्रीपीजी परीक्षा के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अपना स्थान बना लेते हैं। इससे मरीजों के साथ गहन कार्य करने वाले स्थानीय चिकित्सकों को अनावश्यक रूप से प्रतिस्पर्धा में गुजरना होता है।
यहां उल्लेखनीय है कि विदेशी मेडिकल कॉलेज में अधिकांशतया अधोस्नातक विद्यार्थियों को मरीज के साथ बहुत ही सीमित अथवा नगण्य प्रायोगिक अनुभव दिया जाता है। मॉरिशस और नेपाल जैसे कुछ देशों के अपवाद को छोड़ इस बाबत वहां के स्थानीय कानून के साथ-साथ भाषा भी बहुत बड़ा अवरोध साबित होती है। विदेशी मेडिकल कॉलेज से पढ़कर आए विद्यार्थियों में अपेक्षाकृत सैद्धांतिक ज्ञान अधिक होता है क्योंकि वहां संपूर्ण पाठ्यक्रम अधिकांशतया कक्षा में बैठाकर कंप्यूटर, एआइ, ऐनिमेशन इत्यादि संसाधनों से पूर्ण करवाया जाता है। वैसे चिकित्सकीय ज्ञान में सदैव प्रायोगिक पक्ष को सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हर मरीज अलग होता है, हर बीमारी की जटिलता अलग होती है और वह हर बार नए लक्षणों के साथ प्रस्तुत होती है। ऐसे में मात्र सैद्धांतिक ज्ञान से बनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टीसेस (एसओपी) द्वारा मरीज का तर्कसंगत तरीके से इलाज नहीं किया जा सकता।
अनेकानेक बार यह भी देखा गया है कि ये चिकित्सक मरीज को इंजेक्शन लगाने में भी सक्षम नहीं होते और साथ ही मरीज की सामने प्रस्तुत अवस्था के आधार पर इलाज को परिवर्तित भी नहीं कर पाते हैं। इसका खामियाजा मरीज को उठाना पड़ता है। विडंबना तो यह है कि बिना प्रायोगिक ज्ञान वाले ये चिकित्सक कम वेतन पर उपलब्ध हो जाते हैं, परिणामस्वरूप निजी चिकित्सालयों द्वारा इनकी तैनाती गहन चिकित्सा इकाई जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर भी कर दी जाती है। विगत 10 वर्षों में सरकारी पहल पर हर जिले में न्यूनतम एक मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की कवायद की जा रही है। इस सकारात्मक पहल का भी एक पक्ष यह कहते हुए विरोध करता है कि संचालन हेतु उपयुक्त संकाय सदस्य उपलब्ध नहीं है या फिर उनकी गुणवत्ता को लेकर प्रश्न खड़े किए जाते हैं। विरोध करने वालों में कुछ पक्ष इन सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्नातकों की गुणवत्ता को लेकर भी आशंकाएं जताते रहते हैं, लेकिन यही पक्ष बिना प्रायोगिक ज्ञान के छोटे देशों से पढ़े चिकित्सकों की गुणवत्ता पर कहीं भी प्रश्नचिह्न नहीं खड़े करता क्योंकि इसके जरिए कम लागत पर उन्हें चिकित्सक उपलब्ध हो जाते हैं।
केंद्र सरकार की इस पहल के तहत संकाय सदस्यों की आपूर्ति हेतु वर्षों से सरकारी चिकित्सा सेवारत चिकित्सकों को कार्य करने हेतु विकल्प प्रदान करके अवसर दिए जा रहे हैं जो कि पूर्णतया तार्किक एवं उचित है। हो सकता है, इन सेवारत चिकित्सकों के पास शिक्षण का अनुभव नहीं हो किंतु सरकारी सेवा में रहते हुए प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों के भार से उत्पन्न गहन समझ उनकी पृष्ठभूमि में रहती है। उस समझ के रहते ये अनुभवी चिकित्सक विद्यार्थियों को सम्यक ज्ञान देने की स्थिति में होते हैं और स्पष्टतापूर्वक मरीजों के साथ व्यवहार एवं इलाज की बारीकियों को समझा पाते हैं। जहां विदेशों में पढ़ा रहे संकाय सदस्यों के बारे में पूर्णतया अनभिज्ञता होती है, वहीं सेवारत चिकित्सक की ज्ञान संबंधी पृष्ठभूमि सर्वविदित होती है। संभवतया हम ‘घर का जोगी जोगणा, आन गांव का सिद्ध’ वाली कहावत के अनुरूप हमारे सेवारत चिकित्सकों को कम कर आंकते हैं और विदेश में अनभिज्ञ व्यक्ति को भी पूर्ण ज्ञानी मान लेते हैं।
भारत में कहीं से भी यानी सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा स्नातक कर रहे विद्यार्थियों का प्रायोगिक ज्ञान स्तर कुछेक विकसित देशों को छोड़कर श्रेष्ठतम होता है। ऐसे में विदेश जा रहे विद्यार्थियों के प्रवाह को लगाम देने के लिए और अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने संबंधी प्रोत्साहन की आवश्यकता है। यदि प्रतिस्पर्धा से डरते हुए एक बाईपास के रूप में इन छोटे देशों में चिकित्सा शिक्षा के लिए जाने वाले विद्यार्थियों को रोका नहीं गया तो वह भविष्य में चिकित्सा क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। विकल्प के तौर पर विदेशों से शिक्षित स्नातकों के प्रायोगिक कौशल का निर्धारण करने संबंधी व्यवस्था कायम की जानी चाहिए, ताकि वे बेहतर तरीके से मरीज का इलाज कर सकें। सुझाव के तौर पर विदेशों से शिक्षित चिकित्सा स्नातकों के लिए भारत में एफएमजी परीक्षा के पश्चात तीन से छह माह का गहन प्रायोगिक पाठ्यक्रम आयोजित होना चाहिए ताकि वे प्रत्यक्ष इलाज में भी दक्ष हो सकें। प्रायोगिक परीक्षा के पश्चात ही उन्हें पंजीकरण योग्य करार दिया जाना चाहिए। इससे वर्तमान में उपलब्ध लगभग 1,25,000 चिकित्सा शिक्षा अवसरों को सहयोग भी मिल जाएगा।
Hindi News / Opinion / छोटे देशों की चिकित्सा शिक्षा गुणवत्ता पर रखनी होगी नजर
यह खबरें भी पढ़ें
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.